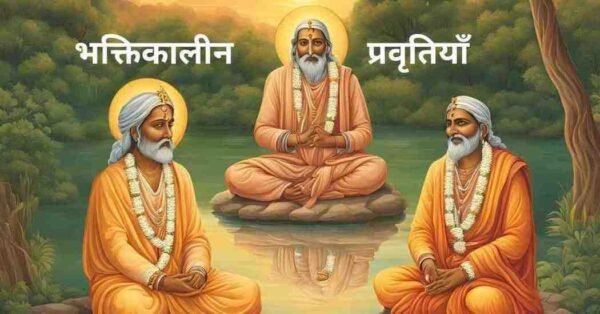भक्तिकाव्य का सारांश:
Bhaktikaal ki visheshtaen अभूतपूर्व हैं इसीलिए इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्तिकाल भारतीय साहित्य इतिहास का एक प्रगतिशील और प्रभावशाली समय था, जिसका समय विशेष रूप से 15वीं से 17वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में संत कवियों ने भक्ति भावना और अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक बदलावों का मार्ग बनाया। भक्तिकाव्य में नाम महिमा, शांत रस, लोक कल्याण और विभिन्न छंदों का प्रयोग जैसी प्रवृत्तियों के माध्यम से भक्ति का प्रचार हुआ। संतों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम को प्रमुखता दी और समाज में व्याप्त असमानताओं, जातिवाद, और भेदभाव का विरोध किया।
आप यहाँ आदिकालीन विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ सकते हैं।
भक्ति भावना की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषता थी, जहाँ संतों ने भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया। गुरु की महिमा और नाम महिमा को महत्व देकर संतों ने गुरु-शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और ईश्वर के नाम स्मरण से मुक्ति की राह दिखाई।
मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति का चित्रण भक्तिकाव्य की एक और विशेषता थी, जहां संत कवियों ने जीवन के मूल्यों, संस्कारों, और संस्कृति को प्रकट किया। जाती-पाती, छुआछूत का विरोध और अहिंसा पर बल देने वाले संतों ने समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। बाह्य आडंबरों का विरोध और विविध मत-मतांतरों का प्रभाव दर्शाता है कि संतों ने धार्मिक आडंबरों को त्यागने और वास्तविक भक्ति मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी।
संत कवियों ने शांत रस का विशेष प्रयोग किया, जिसमें शांति और आत्म-साक्षात्कार की भावना को व्यक्त किया। विविध छंदों के साथ ब्रज और अवधी भाषाओं का प्रयोग भक्तिकाव्य को सरल, सहज और लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। इन भाषाओं में गहराई और लय के साथ संतों ने भक्ति संदेश फैलाया।
अंत में, लोक कल्याण की भावना को प्राथमिकता देते हुए संत कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में समता, न्याय, और प्रेम का प्रचार किया, जिससे समाज में एक सशक्त और समानता पर आधारित संस्कृति की स्थापना हुई। यह काल न केवल भक्ति के स्तर पर, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, और इसके विचार आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं।
भक्तिकाल की विभिन्न प्रवृतियाँ: Bhaktikaal ki visheshtaen
भक्तिकाल को ऐसे ही स्वर्ण युग नहीं कहा जाता क्योंकि भक्तिकाल की विशेषताएँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने में आत्मसात करती हैं इसीलिए वह स्वर्ण युग है।
भक्तिकाल साहित्य का स्वर्णयुग क्यों है। Bhakti kaal sahitya ka swarn yug kyon hai
भक्तिकाल (1375–1700 ई.) हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इस काल में साहित्य ने न केवल काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया बल्कि आम जनमानस की भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया। भक्ति आंदोलन ने साहित्य को एक नई दिशा दी। इस युग में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया।
भक्तिकाल को दो धाराओं में बाँटा जाता है: निर्गुण भक्ति (जैसे कबीर, दादू, रैदास) और सगुण भक्ति (जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा)। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण रूप में पूजा गया, जबकि सगुण भक्ति में राम और कृष्ण जैसे साकार ईश्वर की उपासना हुई।
तुलसीदास ने अपनी कृति ‘रामचरितमानस’ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ लोकजीवन का प्रतिबिंब बना और हिंदू समाज में घर-घर में पढ़ा गया। सूरदास ने ‘सूरसागर’ में बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर वात्सल्य रस की पराकाष्ठा को छुआ। मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर समर्पण और प्रेम की भावना को व्यक्त किया। उनके पद “मेरे तो गिरिधर गोपाल” ने लोकभक्ति को लोकप्रिय बनाया। Bhaktikaal ki visheshtaen अभूतपूर्व हैं। इसी कारण बाबू श्याम सुन्दरदास लिखते हैं कि “जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे कवियों की वाणी देश के कोने कोने में फैली थी। उसे साहित्य में संभवतः भक्तियुग कहते है। निश्चित ही यह हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग था।”1 खुबालकर इस काल में साहित्य ने केवल आध्यात्मिकता का प्रचार नहीं किया बल्कि जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दों पर भी प्रहार किया। इस प्रकार भक्तिकाल ने हिंदी साहित्य को एक समृद्ध, व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण दिया। इसीलिए इस समय को स्वर्णयुग माना जाता है।
भक्तिकाल में भक्ति भावना की प्रधानता Bhaktikal men bhakti bhavna ki pradhanta
Bhaktikaal ki visheshtaen में प्रधान विशेषता है भक्ति जिसे भक्ति काल की आत्मा कहा जा सकता है। भक्तिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता भक्ति भावना की प्रधानता थी। इस काल में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को सर्वोपरि माना गया। भक्ति भावना को दो धाराओं में विभाजित किया गया: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानकर उनकी उपासना की गई, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया।
निर्गुण भक्ति में संत कवियों ने ज्ञान, योग और आत्मा-परमात्मा के मिलन को महत्त्व दिया। कबीरदास ने कहा: “जो भूखा भाव से भजे, मेरी भक्ति को ठाव। घृणा मनै जो भजत है, सो नर्क माहिं पड़ाव।” कबीर के इन दोहों में भक्ति का सार भावनाओं की पवित्रता में निहित है। उन्होंने बाहरी आडंबर और मूर्तिपूजा का विरोध करते हुए अंतरात्मा की शुद्धता पर बल दिया।
सगुण भक्ति में राम और कृष्ण जैसे ईश्वर के अवतारों की भक्ति पर जोर दिया गया। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति और मर्यादा का संदेश दिया। सूरदास ने कृष्ण के बालरूप की लीलाओं का वर्णन करते हुए वात्सल्य रस में भक्ति को गहराई दी। उदाहरण के लिए: “मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मोरी मटकी पटकी धमकै, मुसुकि-मुसुकि सब भायो।”
मीरा बाई की भक्ति भावना कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। उनका पद “पायो जी मैंने राम रतन धन पायो” भक्ति के शाश्वत आनंद को दर्शाता है। “इस काल के सभी कवियों ने अपने अपने आराध्य के प्रति अटूट एकनिष्ठ भक्तिभावना का प्रतिपादन किया है।”2 खुबालकर
भक्ति भावना के इस प्रधान स्वर ने समाज में न केवल आध्यात्मिक चेतना का विकास किया, बल्कि जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को भी कम करने का प्रयास किया। भक्तिकाल ने मानवता को आध्यात्मिक प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण का मार्ग दिखाया।
गुरु की महिमा का गान Bhaktikal ke sahitya men guru ki mahima
Bhaktikaal ki visheshtaen में एक विशेषता है गुरु की महिमा। भक्तिकाल के साहित्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया। गुरु को ज्ञान का स्रोत, आध्यात्मिक पथ का मार्गदर्शक और ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना गया। गुरु की महिमा इस युग में इतनी प्रमुख थी कि उसे ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया। संत कवियों का मत था कि गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा: “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।”
इस दोहे में कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हों, तो पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग दिखाया। कबीर के गुरु के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि “रामानदजी के माहात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगाना घाट सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानदजी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानदजी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानन्दजी बोल उठे ‘राम राम कह’ कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानन्दजी का शिष्य कहने लगे।”3 रामचंद्र शुक्ल कबीर द्वारा गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ भक्ति का मार्गदर्शक माना गया। नानकदेव ने भी गुरु को ईश्वर के समान महत्व देते हुए कहा: “गुरु बिन ज्ञान न होई।” इसका अर्थ है कि गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है।
गुरु शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सगुण भक्ति के कवि तुलसीदास ने भी गुरु को उच्च स्थान दिया। उन्होंने लिखा: “श्री गुरु पद नख मणि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती।” यहाँ तुलसीदास ने गुरु के चरणों को रत्नों के समान बताया है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। मीरा बाई ने भी अपने भजनों में संत रैदास को गुरु मानते हुए उनकी महिमा का गान किया। गुरु की शिक्षाओं ने मीरा को कृष्ण के प्रति समर्पित किया और उनकी भक्ति को नया आयाम दिया।
भक्तिकाल के इस गुरु महत्त्व ने समाज को यह संदेश दिया कि जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु न केवल व्यक्तिगत विकास का स्रोत है, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है।
भक्तिकाल में नाम की महिमा Bhaktikal men naam smaran ka mahatva
नाम की महिमा भी Bhaktikaal ki visheshtaen में से एक है।भक्तिकाल के साहित्य में “नाम महिमा” का विशेष महत्व है। नाम महिमा का अर्थ है—ईश्वर के नाम का स्मरण और जाप करना, जो भक्तों के लिए मोक्ष का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। संत कवियों का मानना था कि ईश्वर के नाम का स्मरण करना किसी भी जप, तप या यज्ञ से श्रेष्ठ है। कबीरदास ने नाम महिमा पर विशेष जोर देते हुए कहा: “सुमिरन कर ले मेरे मनवा, सुमिरन से सब काज। नारद, शुक, सनकादिक, सुमिरन से सब साज।” इसमें कबीर ने नाम-स्मरण को इतना शक्तिशाली बताया कि इससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उनके विचार में, नाम-स्मरण से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर से जुड़ता है।
तुलसीदास ने रामचरितमानस में नाम महिमा को सर्वोपरि बताते हुए लिखा: “नामु कामतरु कालहु छबी। सुमिरत सकल सुलभ फल रबी।” यहाँ उन्होंने राम के नाम को कल्पवृक्ष के समान बताया है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तुलसीदास ने राम के नाम को इतना प्रभावशाली माना कि इसे स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
मीरा बाई ने भी कृष्ण के नाम को अपनी भक्ति का आधार बनाया। उनके भजन “पायो जी मैंने राम रतन धन पायो” में ईश्वर के नाम का स्मरण एक अद्भुत आत्मिक संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। मीरा के लिए कृष्ण का नाम ही जीवन का सर्वस्व था।
संत रैदास ने भी कहा: “हरि का नाम जापते, मिटें पाप के लेख। जैसे पावन गंग जल, हरै मलिन विवेक।” रैदास के अनुसार, ईश्वर के नाम का स्मरण गंगा के पवित्र जल के समान है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। नाम महिमा की इस प्रवृत्ति ने भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया। यह सरल और सुलभ मार्ग था, जो जाति, पंथ और साधन की सीमाओं को तोड़कर ईश्वर से जुड़ने का साधन बना।
भक्तिकाल के साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रकट हुआ। संत कवियों ने भक्ति को केवल ईश्वर-आराधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनुष्य की गरिमा, समानता और प्रेम पर भी बल दिया। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना और जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों को अस्वीकार किया।
कबीरदास ने मानवतावाद की पराकाष्ठा को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया। उनके विचार में, मनुष्य का आचरण और मानवता का पालन ही सच्ची भक्ति है। कबीर कहते हैं: “जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।” इसमें कबीर ने जाति-व्यवस्था का विरोध करते हुए ज्ञान और कर्म को अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार, मनुष्य का मूल्य उसके ज्ञान और कर्म से तय होता है, न कि उसकी जाति से।
रैदास ने भी मानवतावाद पर बल दिया। उन्होंने कहा: “मन चंगा तो कठौती में गंगा।” रैदास का यह कथन बताता है कि यदि मनुष्य का मन पवित्र और निष्कलंक है, तो उसे बाहरी तीर्थयात्राओं या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। यह मानवता की प्रधानता को दर्शाता है। सगुण भक्ति के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में मानवता और मर्यादा को राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र मानव जीवन के लिए आदर्श है। राम का मानवतावादी दृष्टिकोण उनके व्यवहार, वचन और कर्मों में प्रकट होता है। मीरा बाई की भक्ति में भी मानव प्रेम और सहिष्णुता की भावना दिखाई देती है। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति प्रेम, हर व्यक्ति के प्रति समानता का संदेश देता है।
भक्तिकाल ने समाज में यह विचार स्थापित किया कि हर मनुष्य समान है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। मानवतावाद की इस भावना ने समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का कार्य किया।
भारतीय संस्कृति का चित्रण Bhaktikalin sahitya men bhartiya Sanskriti ka chitran
भक्तिकाल के साहित्य में भारतीय संस्कृति का अद्भुत और व्यापक चित्रण मिलता है। इस काल में रचे गए साहित्य ने न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन को अभिव्यक्ति दी, बल्कि समाज, परंपराओं, रीति-रिवाजों और मानवीय मूल्यों का चित्रण भी किया।
तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में आदर्श पारिवारिक जीवन, सामाजिक मर्यादा, धर्म की परिभाषा और नैतिकता के मानदंड स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए हैं। राम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को व्यक्त किया। राम का वनवास, भरत का त्याग, और सीता का समर्पण भारतीय जीवन मूल्यों को दर्शाता है।
सूरदास की सूरसागर में कृष्ण के बाललीलाओं और रासलीलाओं के माध्यम से ब्रज संस्कृति का मनमोहक चित्रण किया गया। उनकी रचनाएँ भारतीय ग्राम्य जीवन, व्रज की गोप-गोपियों की भक्ति और त्योहारों की उल्लासपूर्ण झलक देती हैं। उदाहरण के लिए: “मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो।” यहाँ कृष्ण और उनके मित्रों की लीलाओं में भारतीय समाज के ग्रामीण जीवन का सजीव वर्णन मिलता है।
मीरा बाई की रचनाओं में भी राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। उनके भजन प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना को व्यक्त करते हैं, जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत गुण हैं। संत रैदास और कबीरदास ने भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता को सरल भाषा में व्यक्त किया। उन्होंने आडंबरों और पाखंड का विरोध करते हुए प्रेम, समानता और सेवा को भारतीय संस्कृति का आधार बताया।
भक्तिकालीन साहित्य की सांस्कृतिक व्यापकता पर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि “भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। अत: उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया।”4 विश्वनाथ त्रिपाठी अत: कहना न होगा कि भक्तिकाल का साहित्य भारतीय संस्कृति के हर पहलू—भक्ति, धर्म, मानवता, पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिकता—को उभारता है। यह साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है, जिसने सदियों तक समाज को दिशा प्रदान की।
जाति-पाँति और छुआछूत का विरोध Bhaktikal men jati pati aur chhuaa-chhoot ka virodh
भक्तिकाल के साहित्य में जाति-पाँति और छुआछूत के विरोध का भाव विशेष रूप से प्रकट हुआ। यह काल सामाजिक असमानता और भेदभाव से त्रस्त समाज में समानता और भाईचारे का संदेश लेकर आया। संत कवियों ने जातिगत भेदभाव को कठोरता से नकारा और सभी मनुष्यों को समान बताया। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि “निर्गुण धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्णव्यवस्था की पीड़ा सही थी। अत: उनमें वर्णव्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है।”5 विश्वनाथ त्रिपाठी कबीरदास जाति-पाँति और छुआछूत के सबसे प्रखर आलोचक थे। उन्होंने अपने दोहों में बार-बार जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका दोहा प्रसिद्ध है: “जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।” कबीर ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और ज्ञान से निर्धारित होता है, न कि उसकी जाति से। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं।
रैदास, जो स्वयं एक दलित परिवार से थे, ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनके अनुसार, भक्ति के मार्ग में जाति कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा: “प्रेम भक्ति मग सुखदाई, सब कहूँ सिरमोर। जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई।” इसमें उन्होंने यह संदेश दिया कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, वह सीधे हरि का प्रिय हो जाता है।
सगुण भक्ति के कवि तुलसीदास ने भी जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने लिखा: “ढोल, गवाँर, शूद्र, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।” यद्यपि इस चौपाई को लेकर विवाद होता है, लेकिन तुलसी का समग्र दृष्टिकोण देखें तो उनका रामराज्य सबके लिए समानता और न्याय का आदर्श है।
मीरा बाई ने कृष्ण की भक्ति में जाति को कभी बाधा नहीं बनने दिया। उनके लिए हर व्यक्ति का अधिकार था कि वह भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़े। इस प्रकार, भक्तिकाल ने जाति-पाँति और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। इसने समाज को यह संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग सबके लिए समान है और सभी मनुष्य एक ईश्वर के रूप में जुड़े हुए हैं।
अहिंसा पर बल Bhaktikal men ahinsa par bal diya gaya
भक्तिकाल के साहित्य में अहिंसा को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संत कवियों ने अहिंसा को न केवल शारीरिक हिंसा से मुक्ति के रूप में देखा, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाने की शिक्षा दी। इस प्रवृत्ति का उद्देश्य समाज में शांति और सहिष्णुता का वातावरण बनाना था।
कबीरदास ने अहिंसा को भक्ति का एक प्रमुख आधार बताया। उनका मानना था कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी को भी पीड़ा पहुँचाना पाप है। उन्होंने कहा: “साईं के सब जीव हैं, काहे को मारत माहि। अभय दान सब को दिया, जो हम सन्मुख आहि।” कबीर का यह दोहा स्पष्ट करता है कि सभी जीव ईश्वर की रचना हैं, और किसी भी रूप में हिंसा करना ईश्वर का अपमान है।
नानकदेव ने भी अहिंसा को मानवता का आधार माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर के सच्चे भक्त वही हैं, जो अपने मन और कर्म से हिंसा का त्याग करते हैं और प्रेम और दया का व्यवहार अपनाते हैं। नानक का प्रसिद्ध कथन है: “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरति महत।” इसमें प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दी गई है।
संत रैदास ने भी अहिंसा पर बल दिया। उनके अनुसार, प्रेम और करुणा के बिना भक्ति अधूरी है। उन्होंने कहा: “ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिलै सबन को अन्न। छोट-बड़ो सब सम बसैं, रैदास रहै प्रसन्न।” यह विचार सामाजिक और व्यक्तिगत अहिंसा की भावना को दर्शाता है। सगुण भक्ति के कवि तुलसीदास ने अहिंसा को धर्म का आधार बताया। रामचरितमानस में उन्होंने राम को ऐसे आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया, जो प्रजा के साथ करुणा और न्याय से व्यवहार करते हैं।
भक्तिकाल में अहिंसा को केवल व्यक्तिगत मूल्य तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि यह समाज के सुधार का माध्यम बनी। संत कवियों ने अहिंसा को धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जीवन का मूल आधार बताया।
बाह्य आडंबरों का विरोध Bhaktikalin kaviyon dvara bahya aadambaron ka virodh kiya gaya
भक्तिकाल के साहित्य में बाह्य आडंबरों और पाखंड का कड़ा विरोध किया गया। संत कवियों ने दिखावटी कर्मकांड, मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, यज्ञ, और अन्य बाहरी धार्मिक क्रियाओं को भक्ति का अनिवार्य साधन मानने से इंकार किया। उन्होंने भक्ति को हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम के रूप में परिभाषित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संदर्भ में लिखते हैं कि “उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझा कर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया।”6 51 रामचंद्र शुक्ल संभवतः इसीलिए निर्गुण संतों द्वारा बाह्य आडंबरों का सर्वाधिक विरोध भी हुआ है।
कबीरदास ने अपने दोहों में धार्मिक पाखंड पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं की धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और कहा: “माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मनका छोड़ दे, मन का मनका फेर।” यह दोहा बताता है कि माला घुमाने और बाहरी आडंबर करने से आत्मिक शुद्धि संभव नहीं है। कबीर के अनुसार, सच्ची भक्ति अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी दिखावे से।
नानकदेव ने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने धर्म को सरल और सच्चे प्रेम पर आधारित बताया। उनका कथन है: “मन तो जोति सरूप है, अपना मूल पछान।” नानक का यह विचार बताता है कि ईश्वर को बाहर तलाशने के बजाय, उसे अपने भीतर पहचानने की आवश्यकता है।
भक्तिकाल के कवियों ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग न तो तीर्थयात्रा में है और न ही पूजा के विधि-विधान में। सच्ची भक्ति प्रेम, सहानुभूति, और आत्मा की शुद्धता में है। इस प्रकार, उन्होंने बाह्य आडंबरों को छोड़कर सच्चे आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया।
विभिन्न मत-मतांतरों का प्रभाव Bhaktikalin sahitya par vibhinn maton ka prabhav pada
भक्तिकाल में विभिन्न मत-मतांतरों का गहरा प्रभाव देखा गया। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार “भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से चार प्रमुख संप्रदाय है।”7 14 इस काल में भक्ति आंदोलन ने हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच एक पुल बनाने का कार्य किया, जिसमें योग, वेदांत, सूफी परंपरा, और तंत्र के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह युग धार्मिक सहिष्णुता और विचारों की विविधता को स्वीकार करने का प्रतीक बना।
- वेदांत का प्रभाव: वेदांत दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, ने संत कवियों को गहराई से प्रभावित किया। अद्वैत वेदांत के अनुसार, ईश्वर और जीव एक हैं। संत कबीर ने अद्वैत वेदांत के प्रभाव से कहा: “पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि-सुनि आवै हाँसी।” कबीर के इस दोहे में वेदांत का प्रभाव स्पष्ट है, जहाँ ईश्वर को हर जगह उपस्थित बताया गया है।
- सूफीवाद का प्रभाव: भक्तिकाल में सूफीवाद का भी गहरा प्रभाव देखा गया। सूफी परंपरा में ईश्वर को प्रेम और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सूफी संतों की तरह कबीर और रैदास ने प्रेम और समर्पण को भक्ति का आधार बनाया। कबीरदास के इस दोहे में सूफी विचारधारा झलकती है: “हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या।”
- नाथपंथ और योग का प्रभाव: नाथपंथ और हठयोग की परंपरा भी संत कवियों के चिंतन में गहराई से समाई हुई थी। नाथ योगियों की तरह संतों ने शरीर को साधना का माध्यम माना। संत कवियों ने सहज योग और अंतर्ज्ञान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर बल दिया। कबीर कहते हैं: “साधो, यह तन थाथ न थायी। कंचन का यह देह बनायो, भीतर जात दिखाई।”
- धर्मों का समन्वय: संत कवियों ने हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। कबीरदास ने कहा: “हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दोऊ लड़ी-लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना।”
भक्तिकाल के कवियों ने विभिन्न मत-मतांतरों के विचारों को आत्मसात कर एक नई आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साहित्य में वेदांत, सूफीवाद, योग, और तंत्र के विचार एक साथ समाहित होकर भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने में सहायक बने।
शांत रस का विशेष प्रयोग Bhaktikalin sahitya men shant ras pardhaan raha
भक्तिकाल के साहित्य में शांत रस का विशेष प्रयोग हुआ है। शांत रस वह भाव है, जिसमें मनुष्य सांसारिक मोह-माया, द्वेष, और हिंसा से मुक्त होकर आत्मिक शांति और ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। संत कवियों ने शांत रस का उपयोग मानव मन को आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करने के लिए किया।
- कबीरदास: कबीर के दोहों में शांत रस की प्रधानता है। उन्होंने सांसारिक भौतिकता और झगड़ों को त्यागने पर बल दिया। उनके अनुसार, जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में लीन होता है, वह सच्ची शांति पाता है। “जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। कह कबीर तहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है भगवान।” इसमें कबीर सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर आत्मिक शांति प्राप्त करने का संदेश देते हैं।
- तुलसीदास: तुलसीदास ने रामचरितमानस में शांत रस का गहन प्रयोग किया। उन्होंने भगवान राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से आत्मिक शांति और मर्यादा की शिक्षा दी। राम का वनवास, उनका त्याग और धैर्य शांत रस का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं: “सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी।” यह पंक्ति व्यक्ति को अहंकार त्यागकर पूरे जगत को ईश्वरमय मानने का संदेश देती है।
- सूरदास: सूरदास की रचनाओं में कृष्ण की बाललीलाओं के माध्यम से शांत रस व्यक्त होता है। उनके भजनों में प्रेम, भक्ति, और मन की शांति की झलक मिलती है। उदाहरण: “मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो।” यह भजन सरलता और आंतरिक शांति का अनुभव कराता है।
- रैदास: रैदास के भजनों में शांत रस प्रमुख है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को आत्मा की शांति का सर्वोत्तम मार्ग बताया। “प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय।”
शांत रस ने भक्तिकाल के साहित्य को सौंदर्य और गहराई प्रदान की। इसने आत्मा की शुद्धि और सांसारिक मोह-माया से मुक्ति का मार्ग दिखाया। संत कवियों ने शांत रस के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी।
विविध छंदों का प्रयोग Bhaktikal men vividh chhandon ka prayog hua
भक्तिकाल के साहित्य में विविध छंदों का प्रयोग हुआ, जिससे कवियों ने अपनी रचनाओं में लय और संगीत का संचार किया। छंदों का प्रयोग न केवल काव्य को शास्त्रीय रूप प्रदान करता था, बल्कि भक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में भी सहायक था। संत कवियों ने छंदों का चयन करते समय शब्दों की लय, ध्वनि, और अर्थ की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया।
- तुलसीदास: तुलसीदास ने रामचरितमानस और अन्य रचनाओं में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। उन्होंने कवितावली, हाइकु, चौपाई, दोहा, सोरठा आदि का भरपूर इस्तेमाल किया। तुलसीदास का चौपाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने राम के आदर्शों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। उदाहरण स्वरूप, रामचरितमानस की चौपाई: “धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपदकाल परखिए चारी।” यह छंद न केवल सुंदर लयबद्ध है, बल्कि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किया गया है।
- सूरदास: सूरदास ने अपनी रचनाओं में सोरठा और दोहा का उपयोग किया। उनका काव्य रूप मुख्यतः कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का चित्रण करता है, जिसमें छंदों का प्रयोग भक्ति और प्रेम के भावों को प्रकट करने के लिए किया गया। सूरदास की एक प्रसिद्ध सोरठा: “कृष्ण कन्हैया की बांसुरी, मुरली की आवाज। सुनके डूबे मन के दाम, न जाने ये क्या राज।”
- कबीरदास: कबीर ने दोहा और साखी में छंदों का प्रयोग किया। उनके दोहे सटीक और संक्षिप्त होते हुए भी गहरे अर्थ वाले होते थे, जो सरलता से जनता तक पहुँच जाते थे। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा: “बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।” कबीर का यह दोहा आत्मा की शुद्धता और मानवता का संदेश देता है, जो उनकी काव्यात्मक शक्ति को दर्शाता है।
- रैदास: रैदास ने भी दोहा और साखी छंदों का प्रयोग किया। उनके भजन सरल और दिल को छूने वाले होते थे। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है: “तुमा सो मैं, मैं सो तुम, ये है भक्ति का प्याला। जो साधु सच्चा देखे, वही सच्चा वाला।” रैदास के ये दोहे भक्ति की सरलता और सच्चाई को दर्शाते हैं।
- मीरा बाई: मीरा बाई ने पद, दोहा, और चौपाई छंदों का प्रयोग अपने भजनों में किया। मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति उनके अनुपम प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया गया है। उनका एक प्रसिद्ध पद: “प्यारी मीरा का राधा के संग, नाचे कृष्ण के संग। राजसी हृदय में प्रेम नृत्य, प्यार का अद्भुत रंग।”
भक्तिकाल में छंदों का प्रयोग संत कवियों द्वारा कविता को संगीत, भाव और अर्थ के साथ प्रस्तुत करने के एक प्रभावी तरीके के रूप में किया गया। इन छंदों के माध्यम से उन्होंने भक्ति के संदेशों को अधिक प्रभावशाली और प्रभावी तरीके से जन-जन तक पहुँचाया। छंदों की विविधता ने उनकी काव्य कला को अद्वितीय बनाया और भक्तिकाव्य को शास्त्रीय रूप से समृद्ध किया।
ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग Bhaktikal kaviyon dvara Braj aur awadhi bhasha ka prayog kiya gaya
भक्तिकाव्य में ब्रज और अवधी भाषाओं का विशेष महत्व था। संत कवियों ने इन भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, जिससे उनकी भक्ति भावना को लोक-जन तक सरलता से पहुँचाया जा सके। इसीलिए “भक्तिकालीन कवियों ने ब्रज एवं अवधी भाषा को को ही अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया।”8 285 खुबालकर इन भाषाओं में गहरी सांगीतिक लय और सरलता थी, जो भक्तों के हृदय को सीधे छू जाती थी।
- ब्रज भाषा का प्रयोग: ब्रज भाषा का प्रमुख उपयोग कृष्ण भक्ति में हुआ। यह भाषा विशेष रूप से कृष्ण की लीलाओं, उनके बालरूप, और गोवर्धन पर्वत की पूजा आदि से जुड़ी रचनाओं में देखी जाती है। सूरदास और मीरा बाई जैसे कवियों ने ब्रज भाषा का समृद्ध प्रयोग किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएँ कीं, और उनके द्वारा रचित सूरसागर में कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा में उनके गीतों की सरलता और माधुर्य ने कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बना दिया। सूरदास का एक प्रसिद्ध भजन है: “माता मोरी मैं नहीं माखन खायो। माझा में खेले कृष्णा, राधा के संग नाच्यो।” यह भजन कृष्ण के बचपन की लीलाओं और उनकी मस्तमौला जीवन शैली को व्यक्त करता है, जो ब्रज भाषा की मिठास से भरा हुआ है।
- अवधी भाषा का प्रयोग: अवधी भाषा का प्रमुख प्रयोग तुलसीदास ने किया, विशेषकर अपनी प्रसिद्ध रचनाओं रामचरितमानस और कवितावली में। अवधी भाषा की सरसता और मधुरता ने राम के आदर्शों को आम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुलसीदास की रचनाओं में अवधी का प्रयोग गहरी भक्तिमय भावना और जनसाधारण के लिए सरलता से समझने योग्य था। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है: “श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन, हरण भवभय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंज अरुणं।” यह पंक्ति राम के रूप में अवधी भाषा की सुंदरता और भक्तिपूर्वक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को दर्शाती है।
- मीरा बाई ने भी अपने भजनों में ब्रज और अवधी दोनों का मिश्रण किया। उनके भजन कृष्ण भक्ति के प्रति उनके अविचल प्रेम को प्रकट करते हैं, जो ब्रज भाषा की सरलता और अवधी के भक्ति रस में बहे हुए होते हैं। उनका प्रसिद्ध भजन: “प्यारी मीरा का राधा के संग, नाचे कृष्ण के संग।” इसमें ब्रज और अवधी दोनों की छायाएँ देखने को मिलती हैं।
ब्रज और अवधी भाषाओं का प्रयोग भक्तिकाव्य को सहज और सर्वसमावेशी बनाने का कारण बना। इन भाषाओं की काव्यात्मक लय और साधारणता ने भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया। विशेष रूप से कृष्ण भक्ति में ब्रज भाषा और राम भक्ति में अवधी भाषा का प्रयोग अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। इन भाषाओं ने संतों की रचनाओं को लोकप्रवृत्तियों से जोड़ा और भक्ति को आम जनता तक पहुँचाया।
लोक कल्याण की भावना Bhaktikalin sabhi kaviyon dvaara lok kalyan ki bhavna ka mahatv diya gaya
भक्तिकाव्य में लोक कल्याण की भावना केंद्रीय स्थान रखती थी। संत कवियों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के व्यापक कल्याण के लिए भी अपना साहित्य रचा। उन्होंने धर्म, समाज और आस्था के क्षेत्र में फैले भेदभाव, असमानता और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया और एक सशक्त, समान और समर्पित समाज की कल्पना की।
- समाज सुधार और धर्म के प्रति दृष्टिकोण: संत कवियों ने सामाजिक असमानताओं को उजागर किया और अपने साहित्य के माध्यम से समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। कबीरदास ने भक्ति के माध्यम से जातिवाद, कर्मकांड, और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और धार्मिक आडंबरों की आलोचना की और हर किसी को समान अधिकार देने की बात की। उनका प्रसिद्ध दोहा है: “मुल्ला को मुसलमान, पंडित को हिंदू कहाय। काहे को डरते हैं कबीर, दोनों को एक बड़ाई।” यह दोहा जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उनके विचारों को दर्शाता है।
- समानता और मानवता का संदेश: नानकदेव ने भी लोक कल्याण की भावना को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने समाज में समरसता, धर्म, और मानवता का संदेश दिया। उनका संदेश था कि सभी इंसान एक ही ईश्वर के बनाए हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा: “एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निरभऊ, निरवैर।” नानक के इस संदेश में भगवान की एकता और सभी प्राणियों के बीच भेदभाव न करने की बात की गई है। उनका यह विचार समाज में सच्चे समानता और भाईचारे की भावना को प्रकट करता है।
- संत रैदास का योगदान: रैदास ने भी अपने भजनों में समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों की बात की। उन्होंने न केवल जातिवाद, बल्कि शोषण और असमानता का भी विरोध किया। उनका एक प्रसिद्ध भजन है: “मंत्र से नहीं मन से, होवे तेरो भला। सच्चे दिल से भगवान को, खोज जो सच्चा जला।” रैदास का यह संदेश दर्शाता है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मन, हृदय और कर्म में होनी चाहिए, और हर व्यक्ति का इस भक्ति में बराबरी का अधिकार है।
- शिवाजी और रामदास का योगदान: रामदास ने भी संत व समाज के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और विशेष रूप से उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य जनता के कल्याण की दिशा में था। रामदास के भजनों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उन्होंने व्यक्तिगत मुक्ति के साथ-साथ लोक कल्याण के विचार को भी प्रमुखता दी। इन दोनों के अलावा महाराष्ट्र में नामदेव भी महान भक्त हुए जिनकी कविताओं ने महाराष्ट्र की जनता को मानवतावादी दृष्टि प्रदान की। भक्त नामदेव के संदर्भ में शुक्ल कहते हैं कि “महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है।”9 रामचंद्र शुक्ल
- मीरा बाई का दृष्टिकोण: मीरा बाई के भजन भी लोक कल्याण की भावना से ओत-प्रोत थे। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, बल्कि समाज की नारी शक्ति और सम्मान को बढ़ावा देना भी था। मीरा का जीवन और उनके भजन यह बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को समाप्त किया जा सकता है। उनका प्रसिद्ध भजन है: “प्यारी मीरा का राधा के संग, नाचे कृष्ण के संग।” यह भजन नारी स्वतंत्रता और प्रेम के माध्यम से समाज के कल्याण का संदेश देता है।
निष्कर्ष:
Bhaktikaal ki visheshtaen जो प्रगतिशील और मानवतावाद को महत्व देती है कालांतर में यही विशेषताएँ भारतीय संस्कृति की पहचान बनी। भक्तिकाव्य में लोक कल्याण की भावना का व्यापक प्रभाव था। संत कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को धार्मिक और सामाजिक असमानताओं से मुक्त करने का कार्य किया। उन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और प्रेम का वातावरण बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार, भक्तिकाव्य न केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता था, बल्कि समाज के कल्याण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था।
संदर्भ:
- डॉ. भारती खुबालकर, आधुनिक हिन्दी व्याकरण स्वरुप एवं प्रयोग, साहनी पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 284
- डॉ. भारती खुबालकर, आधुनिक हिन्दी व्याकरण स्वरुप एवं प्रयोग, साहनी पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 284
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2002, पृष्ठ संख्या- 49
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंटल ब्लैकस्वान दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ संख्या- 52
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंटल ब्लैकस्वान दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ संख्या- 32
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2002, पृष्ठ संख्या- 51
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंटल ब्लैकस्वान दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ संख्या- 14
- डॉ. भारती खुबालकर, आधुनिक हिन्दी व्याकरण स्वरुप एवं प्रयोग, साहनी पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 285
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2002, पृष्ठ संख्या- 43