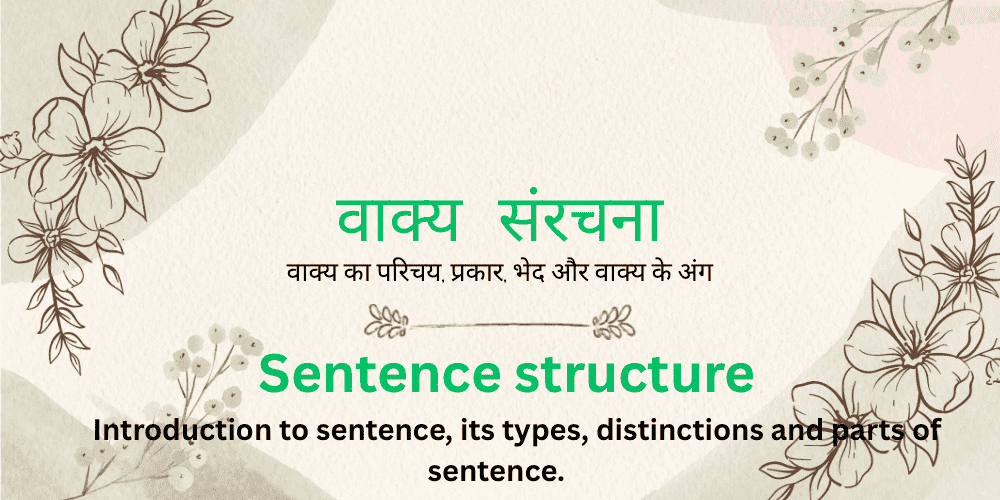वाक्य अनेक शब्दों का समूह (group) है, जो हमारे भावों को स्पष्ट करता है। या कोई निश्चित अर्थ देता है।
Vakya ki paribhasha वाक्य की परिभाषाएँ:
Vakya kise kahate hain इस प्रश्न का उत्तर यदि आसान भाषा में जानना है, तो हमें विद्वानों की परिभाषाओं को आसान बनाना होगा। जैसे कि एक विद्वान कहते है कि शब्दों का एक समूह (Group) जो कोई न कोई अर्थ देता है अथवा मनुष्य के भावों को स्पष्ट करता है, वही वाक्य है। “शब्दों का वह सार्थक समूह, जो किसी न किसी भाव को स्पष्ट करता है, वह वाक्य कहलाता है।”
डॉ. भोलाराम तिवारी के अनुसार: “वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है, जिसमें एक या अधिक शब्द (पद) होते हैं, जो अर्थ एवं भाव की दृष्टि से पूर्ण होता है। जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई न कोई क्रिया आवश्य होती है।” (डॉ. भरती खुबालकर)
आप इसे क्लिक करके हिन्दी पत्र लेखन सीख सकते हैं।
नोट: केवल शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं हो सकता (जैसे- यगरलपनाचना सपालटतक) इसमें शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ नहीं है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ वाक्य के पाँच तत्व बताएँ हैं।
Vakya kise kahate hain जिसमें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पाँच तत्व हो।
सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, समीपता और अन्विति
भारतीय भाषाशास्त्र में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की पूर्णता के लिए पाँच महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार कोई भी वाक्य तभी पूर्ण और व्याकरणिक रूप से सही होता है जब उसमें निम्नलिखित पाँच तत्वों की पूर्ति होती है:
- सार्थकता (Sense / अर्थपूर्णता): वाक्य का अर्थ स्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिए। शब्दों का समूह तभी वाक्य कहलाता है जब उससे कोई स्पष्ट भाव या विचार प्रकट होता हो।
उदाहरण:
- ✅ राम स्कूल गया। (सार्थक – स्पष्ट अर्थ है)
- ❌ स्कूल गया राम। (कम प्रभावी)
- ❌ राम गया स्कूल फल। (असार्थक – अंतिम शब्द अप्रासंगिक है)
स्पष्टीकरण: यदि शब्दों को जोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता या अर्थ भ्रमित होता है, तो वह वाक्य नहीं कहलाता।
- योग्यता (Compatibility / सामर्थ्य): वाक्य के सभी पद (शब्द या उपपद) एक-दूसरे के साथ प्रयोग की दृष्टि से योग्य होने चाहिए। अर्थात प्रसंग के अनुसार भाव बोध होना चाहिए। उनके बीच व्याकरणिक संबंध और भाव-संगति होनी चाहिए।
उदाहरण:
- ✅ गाय घास खाती है। (योग्य प्रयोग – गाय और घास के बीच संबंध स्पष्ट है)
- ❌ किताब पानी पीती है। (अयोग्य प्रयोग – किताब पीने योग्य नहीं है)
स्पष्टीकरण: इस नियम के अनुसार वाक्य में वस्तुगत और भावगत संगति होनी चाहिए। यदि किसी शब्द के साथ प्रयुक्त अन्य शब्द अनुपयुक्त हैं, तो वाक्य भ्रामक हो जाता है।
- आकांक्षा (Expectation / अपेक्षा): वाक्य के प्रत्येक शब्द की एक आकांक्षा होती है और वह किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ने की अपेक्षा करता है जिससे पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो सके। अर्थात् वाक्य में उस शब्द की शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाए।
उदाहरण:
- ❌ राम ने। (अपूर्ण – “ने” से आकांक्षा है कि राम ने क्या किया?)
- ✅ राम ने पुस्तक पढ़ी। (आकांक्षा पूर्ण – पूरा विचार व्यक्त हुआ)
स्पष्टीकरण: यदि किसी शब्द का प्रयोग हो गया है लेकिन उससे जुड़ी अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई, तो वाक्य अधूरा माना जाता है।
- समीपता (Proximity / निकटता): वाक्य में जिन पदों (शब्दों) का आपस में संबंध हो, वे समीप होने चाहिए ताकि अर्थ की स्पष्टता बनी रहे।
उदाहरण:
- ✅ राम ने सीता को फूल दिया।
- ❌ राम ने फूल सीता को दिया। (कम स्पष्टता, शैली में बाधा)
स्पष्टीकरण: वाक्य में यदि संबंधित शब्दों को बहुत दूर-दूर रख दिया जाए, तो अर्थ भ्रमित हो सकता है। समीपता अर्थ की सहजता बनाए रखती है।
- अन्विति (Syntactic Connection / व्याकरणिक संबंध) : वाक्य में सभी शब्दों के बीच उचित व्याकरणिक संबंध होना चाहिए, जैसे कारक, वचन, लिंग, काल आदि। इन सभी का व्याकरण के अनुरूप उचित स्थानों का मेल होना चाहिए।
उदाहरण:
- ✅ सीता खेल रही है। (लिंग, वचन, क्रिया का सामंजस्य है)
- ❌ सीता खेल रहे हैं। (त्रुटिपूर्ण अन्विति – लिंग और क्रिया में मेल नहीं)
स्पष्टीकरण: यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक मेल नहीं बैठता, तो वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अन्विति एक प्रकार का व्याकरणिक अनुशासन है।
संक्षिप्त सारणी: वाक्य की पाँच आवश्यकताएँ:
| क्रम | तत्व | उद्देश्य | उदाहरण (✅/❌) |
| 1. | सार्थकता | स्पष्ट अर्थ देना | ✅ राम सो रहा है ❌ राम फल गया घर |
| 2. | योग्यता | शब्दों के बीच तार्किक संबंध | ✅ बच्चा दूध पीता है ❌ पत्थर खाना खाता है |
| 3. | आकांक्षा | अपेक्षित शब्दों की पूर्ति | ✅ सीता ने गीत गाया ❌ सीता ने |
| 4. | समीपता | संबंधित शब्दों की निकटता | ✅ उसने मुझे किताब दी ❌ उसने किताब दी मुझे |
| 5. | अन्विति | व्याकरणिक सामंजस्य | ✅ वह खा रहा है ❌ वह खा रहे हैं |
वाक्य के अंग अथवा भाग:
हिन्दी व्याकरण में वाक्य को समझने के लिए उसके दो प्रमुख घटकों उद्देश्य (Subject) और विधेय (Predicate) का ज्ञान आवश्यक है।
✍️ वाक्य के भाग: उद्देश्य और विधेय:
उद्देश्य (Subject) – कर्ता का कार्य:
वाक्य में वह भाग जिससे यह ज्ञात होता है कि कार्य किसने किया है, उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। यह वाक्य का मुख्य कर्ता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है।
🔹 उदाहरण:
- राम खेल रहा है। 👉 यहाँ “राम” वह व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है – उद्देश्य
- बच्चा रो रहा है। 👉 “बच्चा” = उद्देश्य।
विधेय (Predicate) – कर्ता का विवरण या क्रिया:
वाक्य में जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, वह विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया और उससे संबंधित अन्य शब्द होते हैं।
🔸 उदाहरण:
- राम खेल रहा है। 👉 “खेल रहा है” = विधेय
- बच्चा रो रहा है। 👉 “रो रहा है” = विधेय
✅ सरल पहचान कैसे करें?
| वाक्य | उद्देश्य (Subject) | विधेय (Predicate) |
| सीता गया रही है। | सीता | गा रही है। |
| विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। | विद्यार्थी | पढ़ रहे हैं। |
| सूरज उग रहा है। | सूरज | उग रहा है। |
Vakya ke bhed ya Vakya ke prakar वाक्य के भेद:
हिन्दी व्याकरण में वाक्य को उसके रचना, अभिव्यक्ति और भाव के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। नीचे वाक्य के प्रमुख भेदों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:
वाक्य के भेद (Types of Sentences in Hindi)
रचना के आधार पर (On the Basis of Structure):
(क) सरल वाक्य (Simple Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया और विचार हो। अर्थात् एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यह वाक्य स्पष्ट, छोटा और सीधा होता है।
🔹 उदाहरण: राम स्कूल जाता है।/ मैं किताब पढ़ता हूँ।
(ख) संयुक्त वाक्य (Compound Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें दो या अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य संयोजन द्वारा जुड़े हों। इस वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है। ये वाक्य ‘और’, ‘किंतु’, ‘तथा’, ‘परंतु’ आदि से जुड़ते हैं। (दो अथवा दो से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं)
🔹 उदाहरण: वह आया और चला गया। / मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन वह खेल रहा है।
(ग) मिश्र वाक्य (Complex Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य जुड़े हों। उपवाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। इस वाक्य में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें (यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, जब, तब, जैसे ही) आदि सहायक क्रियाएँ होती हैं।
🔹 उदाहरण: जब मैं स्कूल गया, तो वह मिल गया। / जो मेहनत करता है, वही सफल होता है।
आप यहाँ से हिन्दी व्याकरण की पुस्तक ख़रीद सकते हैं।
Arth ke aadhar par vakya ke bhed अभिव्यक्ति अथवा अर्थ के आधार पर (On the Basis of Expression):
अभिव्यक्ति (Expression) के आधार पर हिन्दी में वाक्य के आठ प्रकार माने जाते हैं। ये भेद उस उद्देश्य पर आधारित होते हैं जिससे वाक्य कहा गया है। जैसे: सूचना देना, प्रश्न पूछना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, इच्छा प्रकट करना आदि।
अभिव्यक्ति के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार:
1️⃣ विधानात्मक वाक्य (Assertive Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें कोई बात सामान्य रूप से कही जाती है। इसे निश्चित कथन (Statement) भी कहते हैं।
🔹 उदाहरण: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। / वह मेरा मित्र है।
2️⃣ प्रश्नवाचक वाक्य (Interrogative Sentence): ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अक्सर “क्या”, “क्यों”, “कैसे”, आदि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं।
🔹 उदाहरण: क्या तुम स्कूल गए थे?/ तुम्हारा नाम क्या है?
3️⃣ आज्ञार्थक वाक्य (Imperative Sentence): इसमें आज्ञा, निर्देश, आदेश, या सलाह दी जाती है।
यह वाक्य कर्ता रहित (subject-less) भी हो सकता है।
🔹 उदाहरण: दरवाजा बंद करो।/ कृपया यहाँ आइए।/ चुप रहो।
4️⃣ प्रार्थनावाचक वाक्य (Optative Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामना या अभिलाषा प्रकट हो।
🔹 उदाहरण: ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे।/ आप सदा प्रसन्न रहें।/ काश! मुझे भी मौका मिलता।
5️⃣ विस्मयादिबोधक वाक्य (Exclamatory Sentence): ऐसा वाक्य जो आश्चर्य, खुशी, दुःख, गुस्सा आदि भावनाओं को प्रकट करे।
🔹 उदाहरण: अरे! तुम यहाँ कैसे?/ वाह! क्या सुंदर चित्र है।/ हाय! मैं लुट गया।
6️⃣ निषेधवाचक वाक्य (Negative Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात का निषेध या इंकार किया गया हो। इसमें ‘नहीं’, ‘मत’, ‘अवश्य नहीं’ आदि शब्द आते हैं।
🔹 उदाहरण: मैं स्कूल नहीं गया।/ वहाँ मत जाओ।/ यह काम तुमसे नहीं होगा।
7️⃣ संभावनावाचक वाक्य (Potential Sentence): ऐसा वाक्य जो संभावना, योग्यता, क्षमता या अनुमति को व्यक्त करता है। इसमें “सकता है”, “सकते हैं”, “हो सकता है” जैसे शब्द होते हैं।
🔹 उदाहरण: वह यह काम कर सकता है।/ शायद वह आ जाए।/ तुम यह प्रतियोगिता जीत सकते हो।
8️⃣ विकल्पवाचक वाक्य (Alternative Sentence): ऐसा वाक्य जिसमें दो या अधिक विकल्पों में से चयन या निर्णय का अवसर दिया गया हो।
🔹 उदाहरण: तुम चाय लोगे या कॉफी?/ क्या वह आएगा या तुम जाओगे?
📘 सारांश तालिका:
क्रम प्रकार —— उद्देश्य ——- उदाहरण
- विधानात्मक — सामान्य कथन —- वह स्कूल गया।
- प्रश्नवाचक —- प्रश्न पूछना —- क्या तुम आए?
- आज्ञार्थक —- आदेश / निर्देश —- दरवाजा बंद करो।
- प्रार्थनावाचक —- शुभकामना / इच्छा —- ईश्वर भला करे।
- विस्मयादिबोधक —- भावनात्मक प्रतिक्रिया —- अरे वाह! क्या दृश्य है!
- निषेधवाचक —- इंकार / वर्जना —- मत जाओ।
- संभावनावाचक —- संभावना / —- योग्यता वह आ सकता है।
- विकल्पवाचक —- विकल्प देना—- तुम पढ़ोगे या खेलोगे?
भाव के आधार पर (On the Basis of Emotion)
(क) सकारात्मक वाक्य (Affirmative Sentence): जिसमें स्वीकृति या पुष्टि हो।
🔹 उदाहरण: वह अच्छा गाता है।/ वे स्कूल जा रहे हैं।
(ख) नकारात्मक वाक्य (Negative Sentence): जिसमें अस्वीकृति या निषेध हो।
🔹 उदाहरण: वह अच्छा नहीं गाता।/ मैं स्कूल नहीं गया।