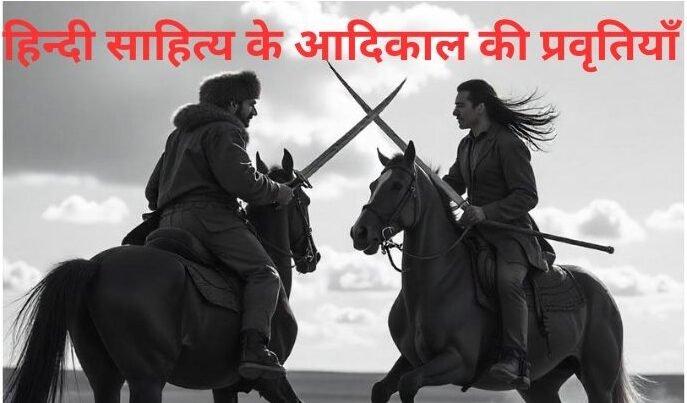Hindi sahitya ka Aadikal हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और आधुनिक काल। इनमें से आदिकाल (1000-1350 ई.) हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक दौर माना जाता है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति वीरगाथा काव्य रचना थी। यह काल मुख्यतः राजपूतों के शौर्य, पराक्रम और युद्धों की घटनाओं को काव्यबद्ध करने का काल था। आदिकाल का साहित्य, विशेषकर वीरगाथा काव्य, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक परिवेश को प्रतिबिंबित करता है।
आप यहाँ हिन्दी साहित्य इतिहास के आदिकालीन विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ सकते हैं।
Hindi sahitya ka Aadikal वीरगाथाओं का वर्णन:
आदिकाल का साहित्य वीर रस से परिपूर्ण है। इसमें राजाओं और योद्धाओं के शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो इस प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के संघर्षों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस साहित्यिक प्रवृत्ति में युद्धों, रणभूमि के दृश्यों और वीर योद्धाओं के अद्भुत साहस की गाथाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। राजाओं के गौरव को बढ़ाने के उद्देश्य से रचनाएँ लिखी गईं।
आदिकाल के साहित्य को ‘वीरगाथा काल’ इसलिए कहा गया, क्योंकि इसमें मुख्यतः राजाओं, वीरों और योद्धाओं की वीरता, शौर्य, युद्ध-कौशल और साहस का वर्णन मिलता है। यह साहित्य मुख्य रूप से राजाओं और सामन्तों के दरबार में रचा गया था और इसमें चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं:
वीर रस की प्रधानता:
इस साहित्य में वीर रस का बाहुल्य है। कवियों ने युद्ध के रोमांचक दृश्य, रणभूमि में सैनिकों का शौर्य, और वीरों के बलिदान का वर्णन किया। कविताओं में वीरता का इतना प्रभाव है कि पढ़ने वाले के मन में उत्साह और गौरव का संचार हो। चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो से यह दोहा पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाता है:
“खग उडि जहँ जहँ जात नृप, बाग उड़ि जहँ जहँ जात।
भूमि गर्ज जहँ जहँ नृप, गाज उठै रघुनाथ।।”
इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है कि उनके जहाँ-जहाँ जाने पर भूमि और आकाश तक उनका प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन है। भोजप्रबंध: राजा भोज के पराक्रम का वर्णन और विजयपाल रासो: गढ़वाल के राजा विजयपाल की वीरता पर आधारित वीर रस प्रधान ग्रंथ है।
राजपूत नायकों का महिमामंडन:
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में राजपूत नायकों का महिमामंडन साहित्य का प्रमुख विषय था। इस काल के कवियों ने राजपूत वीरों की शौर्य गाथाओं, उनके युद्ध कौशल, और बलिदान को काव्यबद्ध किया। राजपूत योद्धाओं को अतिमानवीय गुणों से युक्त दिखाया गया और उनके शौर्य को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया।
राजपूत योद्धाओं और राजाओं की वीरता का गुणगान इस साहित्य का मुख्य विषय था। इसके कारण पर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते है। कि “वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे-छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है।”1 इसीलिए कवि भी अपने अपने सामंतों का गुणगान करना को ही मुख्य विषय माना। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और नायकों को अतिमानवीय रूप में प्रस्तुत किया। जैसे पृथ्वीराज चौहान, राजा भोज, राणा प्रताप आदि।
राजपूत नायक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देने को सर्वोच्च कर्तव्य मानते थे। कवियों ने उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा, और न्यायप्रियता को विस्तृत रूप में वर्णित किया। उदाहरण के लिए, चंदबरदाई की रचना “पृथ्वीराज रासो” में पृथ्वीराज चौहान को ऐसा नायक दिखाया गया है, जिसने मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को कई बार पराजित किया।
उदाहरण:
“खग हीन गरुड़ ज्यों, ब्याकुल भये गगन माहिं।
मोहम्मद सौं धरम रक्ष, चौहान वीर सुभाय।”
यह पंक्तियाँ पृथ्वीराज की धर्मरक्षा और शौर्य का वर्णन करती हैं। इसी प्रकार, “आल्हा खंड” में आल्हा और ऊदल जैसे राजपूत योद्धाओं की वीरता को अमर कर दिया गया है। युद्ध के दौरान उनकी साहसिकता का चित्रण कुछ इस प्रकार है:
“आल्हा बोले खैंच के, सुन ले ऊदल की बात।
गढ़ कटते पर जान चली, नहीं छोड़ेंगे मात।”
आदिकाल का साहित्य राजाश्रित था, जिसमें राजा और उनके राज्य की प्रशंसा की जाती थी। कवि अपने आश्रयदाता राजा को महान योद्धा और धर्मरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और गौरव का महिमामंडन किया गया है। यह प्रवृत्ति उस समय के राजदरबारों में कवियों को प्रोत्साहन मिलने के कारण विकसित हुई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखे गए छंद में राजा के पराक्रम को महिमामंडित किया गया है:
“पृथ्वीराज परमार लख, रण में बाज समान।
उठे खड्ग जब हाथन में, भागे शत्रु महान।।”
यह छंद बताता है कि राजा पृथ्वीराज के युद्ध कौशल के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते। राजपूत नायक केवल युद्धकला में निपुण नहीं थे, बल्कि उनकी नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, और आत्मसम्मान की भावना भी अद्वितीय थी। राजपूत नायकों का महिमामंडन केवल उनके शौर्य का वर्णन नहीं करता, बल्कि समाज को प्रेरणा देता है। यह साहित्य तत्कालीन समाज के मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, जिसने भारतीय संस्कृति में वीरता की भावना को जीवित रखा।
धार्मिक और नैतिक मूल्यों का चित्रण:
वीरगाथा काव्य में केवल नायकों के युद्ध कौशल और वीरता का ही वर्णन नहीं है, बल्कि उनके धर्म के प्रति निष्ठा, न्यायप्रियता और कर्तव्यनिष्ठा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राजपूत नायक न केवल रणभूमि में पराक्रम दिखाते थे, बल्कि अपनी नैतिकता और धर्मपालन से भी समाज के लिए आदर्श स्थापित करते थे। इस काल में धर्म का गहरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। जैन और बौद्ध धर्म के आदर्श साहित्य में प्रमुखता से उभरे। इस संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि “धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात-अज्ञात साधनाएँ प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था।”2 रचनाओं में धार्मिकता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। जैन मुनियों द्वारा रचित पउमचरियम और कुवलयमाला जैसे ग्रंथों में धर्म और अहिंसा के संदेश मिलते हैं। कविताओं और गाथाओं में नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की गई। जैन कवि सोमदेव द्वारा रचित कुवलयमाला का उदाहरण:
“अहिंसा परमोधर्म: धर्म हिंसा तथैव च।
जीवन को जो सुलभ करे, वही है सच्चा धर्म।।”
यह दोहा धर्म और अहिंसा के आदर्शों पर जोर देता है और नैतिकता की शिक्षा देता है। वीरगाथा काल का साहित्य उस समय के समाज में प्रचलित धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। इसमें नायक अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहते थे। नायकों की यह निष्ठा धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, “पृथ्वीराज रासो” में पृथ्वीराज चौहान को धर्मरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी वीरता केवल शत्रु को पराजित करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्रेरित थी।
उदाहरण:
“धर्मनिष्ठ चौहान कुल, शत्रु सहस नहिं जाय।
सत्य, धर्म, औ न्याय का, सदा करें आदर।”
इसी प्रकार, “आल्हा खंड” में आल्हा और ऊदल अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए जीवन समर्पित करने को तत्पर रहते हैं। वे युद्ध में कर्तव्य और धर्म के पालन को सर्वोपरि मानते थे।
उदाहरण:
“धरम छोड़ि न आल्हा लड़े, चाहे होय प्राण गमाय।
मातृभूमि के कारन, हर कष्ट सहे मुस्काय।”
वीरगाथा काव्य में नायकों को न्यायप्रिय और कर्तव्यपरायण दिखाया गया है। वे सदैव अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनके निर्णय धर्म और न्याय पर आधारित होते थे, जो उस समय के आदर्श शासक की छवि को प्रस्तुत करता है। वीरगाथा काव्य केवल युद्धकला और शौर्य का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों का भी सजीव चित्रण है। इन काव्यों के माध्यम से तत्कालीन समाज में धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा दी गई।
लोकभाषा का प्रयोग:
वीरगाथा काल के साहित्य में लोकभाषा का प्रयोग इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। इस युग में साहित्य का उद्देश्य केवल दरबारी मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना भी था। इसलिए कवियों ने संस्कृत जैसी जटिल भाषा के बजाय लोकभाषाओं का प्रयोग किया। प्रमुख लोकभाषाएँ जैसे अपभ्रंश, ब्रजभाषा, और अवहट्ट का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ। इस काल की भाषा अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी थी। भाषा सरल और छंदबद्ध थी। इसमें दोहा, चौपाई, त्रिपदी आदि छंदों का प्रचलन था। जैसे, चंदबरदाई के दोहे और चौपाइयाँ साहित्यिक शैली की विशेषता हैं। भाषा के दृष्टिकोण से चौपाई का उदाहरण:
“सुरपुर, नरपुर, नागपुर, सब पुकारत एक।
पृथ्वीराज की विजय का, गूँजे तिन्ह लोक।।”
अपभ्रंश का उपयोग: अपभ्रंश, जो संस्कृत और प्राकृत से विकसित हुई थी, वीरगाथा साहित्य की प्रमुख भाषा रही। यह भाषा सरल और जनसामान्य की समझ में आने वाली थी। उदाहरण के लिए, “पृथ्वीराज रासो” में चंदबरदाई ने अपभ्रंश का उपयोग किया।
उदाहरण:
“खग मृग नखग तनु, चौहान हिय दार।
धरम राखि धरती, वीर बली प्रहार।”
यहाँ भाषा में लोकसुलभता दिखाई देती है, जिससे सामान्य लोग भी इसे आसानी से समझ सकते थे।
ब्रजभाषा और अवहट्ट का प्रयोग: ब्रजभाषा और अवहट्ट का उपयोग भी वीरगाथा साहित्य में हुआ। ब्रजभाषा के प्रयोग ने साहित्य को अधिक संगीतमय और प्रभावी बनाया। अवहट्ट का उपयोग विशेषतः युद्ध के दृश्य वर्णन में हुआ। “आल्हा खंड” में ब्रज और अवहट्ट का प्रयोग आल्हा और ऊदल जैसे नायकों की गाथाओं को लोकप्रिय बनाने में सहायक हुआ।
उदाहरण:
“बरछी-बरछा उठाय चले, धरम हेतु रण बांध।
ब्रजमंडल की भूमि बचाय, आल्हा वीर असाध।”
भाषा की सरलता और प्रभाव: वीरगाथा काल की भाषा शैली में सरलता थी, ताकि आम जनमानस इसे समझ सके। भाषा में वीर रस और ओज का प्रयोग इसे और प्रभावी बनाता था। यह साहित्य उस समय के समाज के भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम बना। कहना न होगा कि लोकभाषाओं के उपयोग ने वीरगाथा काव्य को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत बना।
इस काल की भाषा अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी थी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस काल के साहित्य की भाषा को विभिन्न बोलियों की भाषा कहा है। “आदिकाल का हिन्दी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है।”3 भाषा सरल और छंदबद्ध थी। इसमें दोहा, चौपाई, त्रिपदी आदि छंदों का प्रचलन था। जैसे, चंदबरदाई के दोहे और चौपाइयाँ साहित्यिक शैली की विशेषता हैं।
भाषा के दृष्टिकोण से चौपाई का उदाहरण:
“सुरपुर, नरपुर, नागपुर, सब पुकारत एक।
पृथ्वीराज की विजय का, गूँजे तिन्ह लोक।।”
इसमें सरल भाषा और दोहे-चौपाई के माध्यम से राजा की विजय की गाथा प्रस्तुत की गई है।
शौर्य और प्रेम का मिश्रण:
आदिकालीन साहित्य में शौर्य और प्रेम का एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वीरगाथा साहित्य, जो मुख्यतः नायकों के शौर्य और युद्ध-कौशल का वर्णन करता है, उसमें प्रेम के प्रसंग भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह प्रेम न केवल मानवीय भावनाओं का चित्रण करता है, बल्कि नायकों की वीरता को और भी प्रभावी बनाता है।
शौर्य और प्रेम का संतुलन: आदिकालीन साहित्य में प्रेम को नायकों के चरित्र की गहराई बढ़ाने के लिए जोड़ा गया। प्रेम के कारण नायक का व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली और मानवीय बनता है। नायिका के प्रति प्रेम और उसके सम्मान के लिए नायक युद्ध तक करने को तत्पर रहता है। प्रेम केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह नायक की प्रेरणा और साहस का स्रोत भी बनता है। इस संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास में लिखते हैं कि “रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और शृंगार रासो के प्रमुख रस हैं।”4 साथ ही साथ आदिकालीन साहित्य में वीरता के साथ प्रेम का भी चित्रण मिलता है। नायिका-भेद और नायक-नायिका के प्रेम प्रसंगों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। जैसे, पृथ्वीराज रासो में संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम का उल्लेख है।
“देखे रूप संयोगिता, भूले सब योद्धा।
विजयी बने पृथ्वीराज, प्रेम मधुर मीठा।।”
पृथ्वीराज रासो में प्रेम: “पृथ्वीराज रासो” में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा इसका प्रमुख उदाहरण है। चंदबरदाई ने इस प्रेम को रोचक और रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया। संयोगिता का स्वयंवर और पृथ्वीराज द्वारा उसे जीतकर ले जाने की कथा में प्रेम और शौर्य का अनूठा मिश्रण है।
उदाहरण:
“संग्राम भूमि में जिते, नृप पृथ्वीराज महान।
प्रेम-सूत्र संयोगिता, चित्त चढ़ाय स्वाभिमान।”
नायिका-भेद और प्रेम प्रसंग: आदिकालीन साहित्य में नायिका-भेद का भी वर्णन मिलता है। इसमें नायिकाओं के विभिन्न रूप और उनके प्रेम-प्रसंगों को दर्शाया गया। नायक-नायिका के बीच प्रेम के माध्यम से कहानी में भावनात्मक गहराई और रोचकता उत्पन्न की जाती थी।
अत: कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदिकालीन साहित्य में शौर्य और प्रेम का मिश्रण साहित्य को न केवल वीरता का प्रतीक बनाता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी चित्रण करता है। प्रेम और शौर्य के इस संगम ने उस युग के साहित्य को प्रेरणादायक और मनोरंजक बनाया।
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण:
आदिकालीन साहित्य, विशेषकर वीरगाथा काव्य, तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक जीवन का एक प्रभावशाली प्रतिबिंब है। इस साहित्य ने केवल नायकों की वीरता और युद्ध-कौशल को ही नहीं, बल्कि समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों, धार्मिक आस्थाओं, त्योहारों, और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी उकेरा है। यह साहित्य उस समय के जीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है।
सामाजिक जीवन का चित्रण: आदिकाल के साहित्य में तत्कालीन समाज की संरचना और जीवनशैली का सजीव चित्रण मिलता है। यह युग सामंतवादी था, जिसमें राजा और उनके दरबारी समाज के केंद्र थे। राजाओं के दरबारों में निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ, न्याय व्यवस्था, और कूटनीति का वर्णन साहित्य का हिस्सा था। “पृथ्वीराज रासो” और अन्य वीरगाथाओं में राजाओं के सामरिक कौशल, दरबार में उनके निर्णय और प्रजा के कल्याण के लिए उनकी नीतियों का वर्णन मिलता है।
सामाजिक जीवन में युद्ध का प्रमुख स्थान था। योद्धा न केवल समाज के रक्षक थे, बल्कि आदर्श भी माने जाते थे। युद्ध के दौरान सेना की संरचना, शस्त्रों का प्रयोग, और रणनीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है।
उदाहरण:
“गज सजे, घोड़ सजे, वीर चले मैदान।
रचि-रचि पांत खड़े, धरम-रक्षा सदा प्रधान।”
महिलाओं का भी आदिकालीन साहित्य में उल्लेख है। महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया गया, और उनकी भूमिका परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नायिकाएँ केवल प्रेम के प्रसंगों में ही नहीं, बल्कि अपने नायकों को प्रेरित करने और समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
सांस्कृतिक जीवन का चित्रण: आदिकालीन साहित्य में सांस्कृतिक जीवन को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। त्योहार, धार्मिक आयोजन, रीति-रिवाज और परंपराएँ साहित्य में स्पष्ट रूप से झलकती हैं। त्योहारों और उत्सवों का वर्णन जीवन में उल्लास और सामूहिकता की भावना को दर्शाता है। इसी प्रवृत्ति को विश्वनाथ त्रिपाठी मिली-जुली संस्कृति का चित्र कहते है। “हिन्दी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिन्दी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली-जुली संस्कृति का चित्र रहा है।”5
धार्मिक आयोजनों का वर्णन वीरगाथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजाओं और नायकों के लिए धर्म रक्षा सर्वोपरि थी। इस युग में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का बड़ा महत्व था। नायक धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य और न्याय के रक्षक और अधर्म के नाशक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
उदाहरण:
“मंदिर के दीप जलाय, रचि-रचि पूजा थाल।
धर्म करे जयघोष, बढ़े वीरों का मान।”
राजसी परंपराएँ और दरबार: राजाओं के दरबारों में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती थीं। चंदबरदाई जैसे कवि राजाओं के आश्रित थे और उनके शौर्य को अमर बनाने के लिए काव्य रचते थे। यह परंपरा केवल साहित्यिक गौरव का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उस समय की संस्कृति को संरक्षित करने का माध्यम भी थी।
अत: आदिकालीन साहित्य ने तत्कालीन समाज और संस्कृति को व्यापक रूप से चित्रित किया। युद्ध और वीरता के साथ-साथ समाज के त्योहारों, परंपराओं, और धार्मिक आस्थाओं का उल्लेख इसे अधिक सजीव और प्रासंगिक बनाता है। यह साहित्य केवल वीरगाथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।
निष्कर्ष:
इन प्रवृत्तियों के माध्यम से Hindi sahitya ka Aadikal की प्रवृतियों में साहित्य वीरता, धर्म, प्रेम और समाज का प्रतिबिंब है। प्रत्येक प्रवृत्ति तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रकट करती है। आदिकाल के साहित्य में वीरता, प्रेम, धर्म और समाज का संतुलित चित्रण मिलता है। इन कविताओं के माध्यम से उस समय की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। आदिकाल का वीरगाथा साहित्य तत्कालीन समाज में वीरता, साहस और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। यह साहित्य न केवल मनोरंजन का माध्यम था, बल्कि समाज को नैतिक और धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान करता था। वीरगाथा साहित्य ने हिन्दी साहित्य को एक सुदृढ़ आधार दिया, जिस पर आगे चलकर भक्तिकाल और रीतिकाल की साहित्यिक परंपराएँ विकसित हुईं।
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2011, पृष्ठ-10
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2011, पृष्ठ-9
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2011, पृष्ठ-1
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2011, पृष्ठ-7
- विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2011, पृष्ठ-1