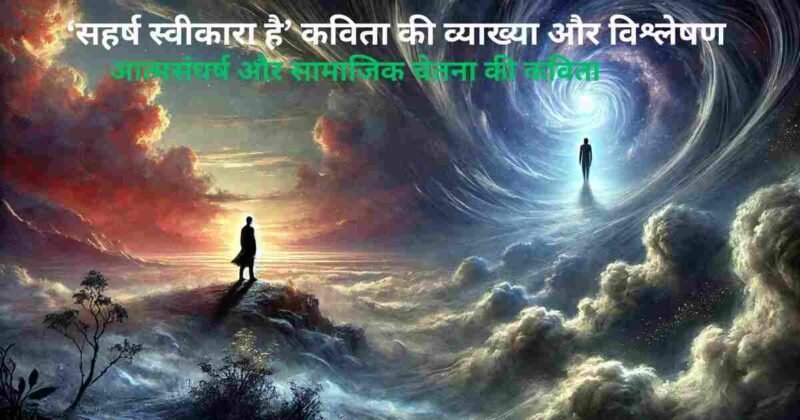सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या जब हम करते हैं तब हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं और वे अपनी कविताओं के लिए कैसी विषय वस्तु का चयन करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है केवल एक आत्मस्वीकृति की ही कविता नहीं है बल्कि यह एक बौद्धिक, दार्शनिक और सामाजिक आत्मनिरीक्षण की कविता भी है।
यहाँ आप ‘नवीन’ की कविता ‘सदा चाँदनी’ की व्याख्या पढ़ सकते हैं।
सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या: आत्मसंघर्ष और सामाजिक चेतना की कविता
“ज़िन्दगी में जो कुछ है, जो भी है
सहर्ष स्वीकारा है;
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
वह तुम्हें प्यारा है।
गरबीली ग़रीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब
यह विचार-वैभव सब
दृढ़्ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब
मौलिक है, मौलिक है
इसलिए के पल-पल में
जो कुछ भी जाग्रत है अपलक है-
संवेदन तुम्हारा है !”
व्याख्या:
मुक्तिबोध की इन पंक्तियों में एक गहरी आत्मस्वीकृति, संघर्षशील जीवन का गौरव और सामाजिक चेतना की प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। कवि अपने जीवन में प्राप्त सभी अनुभवों, चाहे वे सुखद हों या दुखद सभी को “सहर्ष स्वीकारा है”, अर्थात आनंदपूर्वक अपनाते हैं। यहाँ स्वीकृति मात्र बाहरी परिस्थितियों की नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू की है, चाहे वह कठिनाइयाँ हों, गरीबी हो या फिर संघर्ष का अनुभव ही क्यों न हो।
कवि कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी जिया है, भोगा है, वह सिर्फ उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि वह किसी प्रिय व्यक्ति (संकेत रूप में जनता या समाज) के लिए भी मूल्यवान है। “जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है।” यहाँ ‘तुम्हें’ शब्द व्यापक है और इसे पाठक, समाज या साथी विचारधारा के लोग माना जा सकता है।
इसके बाद कवि अपनी “गरबीली ग़रीबी”, “गंभीर अनुभव” और “विचार-वैभव” की बात करते हैं। यहाँ गरीबी केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक संघर्ष का भी प्रतीक हो सकती है। “गंभीर अनुभव” का तात्पर्य उनके विचारों की परिपक्वता और संघर्ष की गहराई से है, जबकि “विचार-वैभव” का तात्पर्य उनकी बौद्धिक संपन्नता से है। यह सब कुछ उनके जीवन की मौलिक उपलब्धियाँ हैं, जिन्हें उन्होंने बिना किसी संकोच के साथ अपनाया है।
कवि आगे कहते हैं कि उनके भीतर एक “सरिता”, अर्थात सतत प्रवाहित विचारों की धारा है। यह उनकी मौलिकता और नवाचार का प्रतीक है। वे अपने भीतर की इस प्रवृत्ति को अनमोल मानते हैं क्योंकि यह निरंतर जागरूकता (consciousness) को जन्म देती है।
अंत में कवि इस पूरी स्वीकृति को “संवेदन तुम्हारा है!” कहकर एक समर्पण की तरह प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका यह विचार-संसार, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी आत्मस्वीकृति आदि सब किसी और के प्रति अर्थात जनता या पाठक वर्ग के प्रति समर्पित है। अत: कहना न होगा कि यह कविता आत्मसंघर्ष और समाज के प्रति समर्पण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।
“जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है
जितना भी उँड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता है
दिल में क्या झरना है?
मीठे पानी का सोता है
भीतर वह, ऊपर तुम
मुसकाता चाँद ज्यों धरती पर रात-भर
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है!”
व्याख्या:
इन पंक्तियों में कवि एक रहस्यमय संबंध की बात कर रहे हैं। उस संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर चित्रण कर रहे हैं।
कवि कहते हैं कि “जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है”, यानी यह कोई साधारण सांसारिक संबंध नहीं बल्कि एक गूढ़ और गहरे स्तर पर महसूस किया जाने वाला संबंध है। यह किसी व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है और व्यापक रूप से समाज या किसी उच्चतर चेतना से भी हो सकता है।
कवि आगे कहते हैं कि वह इस संबंध में जितना भी समर्पित होते हैं, जितना भी प्रेम या संवेदना उँड़ेलते हैं, वह कभी समाप्त नहीं होती बल्कि बार-बार नए रूप में उभर आती है। “जितना भी उँड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता है”। यह प्रेम, संवेदनशीलता और विचारों का अनंत स्रोत दर्शाता है, जो उनके भीतर कभी समाप्त नहीं होता। वे इसे “मीठे पानी का सोता” बताते हैं, जो उनकी आत्मा से स्वतःस्फूर्त रूप में निकलता है। यहाँ पानी का सोता उनके संवेदनशील हृदय, विचारों की गहराई और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है।
कवि कहते हैं कि उनके भीतर यह प्रवाह सतत चलता रहता है लेकिन इसके ऊपर किसी का प्रभाव है। “भीतर वह, ऊपर तुम”। यह पंक्ति संकेत देती है कि यह संवेदना, यह विचारधारा, यह आत्मीयता किसी के प्रभाव से संचालित हो रही है।
अंतिम पंक्तियों में मुक्तिबोध इस गहरे संबंध की तुलना चाँद और धरती से करते हैं। “मुसकाता चाँद ज्यों धरती पर रात-भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है!” यहाँ चाँद और चेहरा एक प्रतीकात्मक रूपक हैं। चाँद, जो रातभर धरती पर अपनी शीतल रोशनी बिखेरता है, उसी तरह कोई प्रिय या प्रेरणास्रोत (जो कवि के लिए समाज, विचारधारा या प्रेम भी हो सकता है) उन पर प्रभाव डालता है। यह प्रेम और प्रेरणा का अटूट स्रोत है। यही स्त्रोत उन्हें सतत ऊर्जा प्रदान करता है।
“सचमुच मुझे दण्ड दो कि भूलूँ मैं भूलूँ मैं
तुम्हें भूल जाने की
दक्षिण ध्रुवी अंधकार-अमावस्या
शरीर पर,चेहरे पर, अंतर में पा लूँ मैं
झेलूँ मै, उसी में नहा लूँ मैं
इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित
रहने का रमणीय यह उजेला अब
सहा नहीं जाता है।
नहीं सहा जाता है।
ममता के बादल की मँडराती कोमलता–
भीतर पिराती है
कमज़ोर और अक्षम अब हो गयी है आत्मा यह
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है
बहलाती सहलाती आत्मीयता बरदाश्त नही होती है !”
व्याख्या:
इन पंक्तियों में कवि एक गहरे मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वे स्वयं को एक कठोर दंड देने की इच्छा जताते हैं क्योंकि वे “तुम्हें भूल जाने की भूल” कर सकें। यहाँ “तुम” का प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई स्मृति या फिर कवि निज आत्मबोध या संवेदनशीलता।
कवि यह दंड इतना कठोर चाहते हैं कि वे एक “दक्षिण ध्रुवी अंधकार-अमावस्या” जैसी स्थिति में पहुँच जाएँ। जहाँ केवल घोर अंधकार हो, कोई प्रकाश न हो और कोई स्मृति भी न रह सके। यह अंधकार उनके पूरे “शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में” छा जाए क्योंकि वे अपने भीतर व्याप्त कोमलता और संवेदनाओं से मुक्त हो सकें।
लेकिन यह स्वीकृति केवल आत्म-भूल की नहीं है बल्कि एक प्रकार के विरोधाभास का भी संकेत है। कवि कहते हैं कि वे पूरे “तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित” हैं। अर्थात वे पूरी तरह उसी भावना, उसी स्मृति, उसी अस्तित्व प्रभाव के अधीन हैं, जिसे वे भूलना चाहते हैं। लेकिन इस रमणीय उजाले को अब सहन करना कठिन हो गया है। यह उजाला, जो कभी आनंददायक था लेकिन अब यही आनंद एक मानसिक बोझ की तरह महसूस हो रहा है, जो ‘नहीं सहा जाता है।’
इसके पश्चात कवि “ममता के बादल की मँडराती कोमलता” का जिक्र करते हैं। यह कोमलता, जो कभी सुखद और आश्रय देने वाली थी वही अब उनके भीतर पीड़ा उत्पन्न कर रही है। संवेदना और आत्मीयता पहले जीवन का आधार थी किंतु अब वही असहनीय बन चुकी है।
अंत में कवि आत्मा की स्थिति को स्वीकारते हैं और लिखते हैं कि “कमज़ोर और अक्षम अब हो गयी है आत्मा यह” अर्थात अब वह संघर्ष और संवेदनाओं के बोझ को झेलने में असमर्थ हो गई है। उसे अब संभावित भविष्य से डर लगने लगता है। “छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है”।
सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति “बहलाती सहलाती आत्मीयता बरदाश्त नहीं होती है!!!” इसका अर्थ है कि अब वह स्नेह, वह अपनापन, जो पहले सुखद था, अब एक मानसिक बोझ बन गया है। यह एक गहरे अस्तित्ववादी संघर्ष को दर्शाता है। जहाँ व्यक्ति अपने ही भावनात्मक बंधनों से मुक्त होना चाहता है लेकिन मुक्त हो नहीं पाता।
“सचमुच मुझे दण्ड दो कि हो जाऊँ
पाताली अँधेरे की गुहाओं में विवरों में
धुएँ के बाद्लों में
बिलकुल मैं लापता!!
लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है!!
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
या मेरा जो होता-सा लगता है, होता सा संभव है
सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है
अब तक तो ज़िन्दगी में जो कुछ था, जो कुछ है
सहर्ष स्वीकारा है
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
वह तुम्हें प्यारा है।”
व्याख्या:
इन पंक्तियों में कवि फिर से आत्मसंघर्ष, गहरे मानसिक द्वंद्व और आत्मसमर्पण की भावना को व्यक्त कर रहे हैं।
वह स्वयं को दंडित करने की इच्छा जताते हैं और वह दंड ऐसा हो कि वह अंधकार में डूब जाएँ। किसी गहरे, अज्ञात, पाताल जैसे स्थान में जहाँ कोई प्रकाश न हो। ‘पाताली अँधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएँ के बादलों में, बिलकुल मैं लापता!!’ यह ‘लापता’ हो जाना एक तरह से स्वयं से पलायन है। पलायन अर्थात एक ऐसी स्थिति जहाँ उनकी अपनी कोई पहचान न बचे। लेकिन इस पलायन का भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जहाँ भी वह जाएँगे, वहाँ भी ‘तुम’ का सहारा रहेगा। ‘लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है!!’
यह “तुम” यहाँ पर एक गहरे संबंध का प्रतीक है। यह कोई प्रिय व्यक्ति, समाज, विचारधारा या चेतना हो सकती है। अर्थात कवि इस भावना से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन वह भावना सर्वव्यापी है जिससे बचा नहीं जा सकता।
फिर कवि कहते हैं कि जो कुछ भी उनका है, जो कुछ भी उनका हो सकता है, वह सब ‘तुम’ के कारण ही संभव है। यहाँ ‘तुम’ एक प्रेरणा-स्रोत भी हो सकता है, जो उनके कार्यों, उनके विचारों और उनके अस्तित्व को संचालित करता है।
अंत में कवि अपने पूरे जीवन के अनुभव को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि “अब तक तो ज़िन्दगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है।” यहाँ “सहर्ष स्वीकारा है” सिर्फ़ जीवन की परिस्थितियों को अपनाने की बात नहीं है बल्कि यह एक गहरे आत्मबोध का प्रतीक है। कवि मानते हैं कि उन्होंने अपने संघर्षों, अपने दर्द, अपने विचारों और अपनी पूरी यात्रा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है।
इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि “जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है।” अर्थात उनके होने का, उनके संघर्षों का, उनके विचारों का महत्व केवल इसीलिए है क्योंकि वह ‘तुम’ के लिए महत्वपूर्ण है।
कठिन शब्दों के अर्थ:
सहर्ष: आनंदपूर्वक joyfully, स्वीकारा: अपनाया, Accepted, गरबीली: स्वाभिमानी, आत्मसम्मान से भरपूर Dignified, self-respecting, गंभीर: गहरी सोच से भरपूर, Serious, वैभव: समृद्धि, Grandeur, दृढ़ता: मज़बूती, Firmness, अभिनव: नया, नवीन Innovative, new, संवेदन: अनुभव, भावना Sensation, emotion, परिवेष्टित: चारों ओर से घिरा हुआ Surrounded, enveloped, आच्छादित: ढका हुआ, Covered, रमणीय: सुंदर, आनंददायक Delightful, picturesque, भवितव्यता: भविष्य की अनिवार्यता, Inevitability, गुहा: गुफ़ा, Cave, विवर: संकरी गुफ़ा, गड्ढा Hollow, crevice, पाताली: बहुत गहरा, धरती के नीचे Underworld, abyssal, आत्मीयता: अपनापन, Intimacy, अक्षम: असमर्थ, Incapable, मँडराना: किसी चीज़ के चारों ओर घूमना To hover, to circle around, कोमलता: नर्मी, सौम्यता Softness, tenderness, पिराना: हल्का दर्द होना, To ache, सहारा: समर्थन, Support
कुछ शब्द प्रतीकात्मक भी हैं जैसे:
- “अमावस्या” यहाँ केवल अंधकारमयी रात का नहीं बल्कि मानसिक अवसाद और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी है।
- “लापता” का अर्थ केवल भौतिक रूप से खो जाना नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व के द्वंद्व में उलझ जाना भी है।
- “धुएँ के बादल” भ्रम, असमंजस और अस्पष्टता का प्रतीक हैं।
सहर्ष स्वीकारा है: आत्मसंघर्ष और सामाजिक चेतना की कविता
कविता का सार:
गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता “सहर्ष स्वीकारा है” उनकी गहन आत्मसंघर्ष, विचारधारा, संवेदनशीलता और समाज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कविता में केवल आत्मनिरीक्षण ही नहीं बल्कि कवि मुक्तिबोध के विचारों, भावनाओं और अस्तित्व के व्यापक विश्लेषण का मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक चेतना का अद्भुत समन्वय है।
कविता की विषय वस्तु और विश्लेषण:
- निज स्वीकार्यता और आत्मसंघर्ष: यह कविता स्वीकार्यता, आत्मसंघर्ष और सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इसमें कवि अपने जीवन के संघर्षों, मानसिक द्वंद्व और एक उच्चतर सत्य की खोज को स्वीकारने का प्रयास करते हैं। वे अपने अनुभवों को नकारने के बजाय उन्हें अपनाते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उनका पूरा अस्तित्व किसी और (संकेत रूप में समाज, विचारधारा या प्रिय व्यक्तित्व) से गहराई से जुड़ा हुआ है।
प्रस्तुत कविता में निज स्वीकृति और आत्मसंघर्ष अर्थात कवि अपनी कमजोरियों और द्वंद्व को भी सहज रूप से स्वीकारते हैं। कवि इतने संवेदनशील हैं कि आत्मीयता और प्रेम भी उनके लिए बोझ बन जाते हैं। कविता में पलायन और वापसी का संघर्ष भी दृष्टिगोचर होता है अर्थात वे अंधकार में खो जाना चाहते हैं लेकिन अंत में वे पाते हैं कि वहाँ भी उनकी स्मृतियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती है। कविता में समाज और विचारधारा की अनिवार्यता का मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि अनुभव करते हैं कि उनकी सारी सोच, उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष किसी बड़ी विचारधारा से जुड़ा हुआ है।
आत्मसंघर्ष और आत्मस्वीकृति:
कवि जीवन की परिस्थितियों, संघर्षों, विचारों और अपने भीतर की बेचैनी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। वे अपनी गरीबी, विचारधारा और अनुभवों को बोझ नहीं मानते बल्कि इसे अपनी आत्मा का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ‘ज़िन्दगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है’ इस पंक्ति में “सहर्ष स्वीकारा है” महज एक वाक्य नहीं है बल्कि यह एक दर्शन को व्यक्त करता है। मुक्तिबोध यह स्वीकारते हैं कि उनके जीवन में जो भी है, चाहे वह गरीबी हो, संघर्ष हो, विचारों की बेचैनी हो सबको उन्हें उसे खुशी-खुशी अपनाना होगा क्योंकि यही उनके अस्तित्व की पहचान है।
पलायन और वापसी का विरोधाभास:
कवि मुक्तिबोध प्रस्तुत कविता में अपने भीतर पलायन की इच्छा को व्यक्त करते हैं। वे खुद को अंधकार में दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या में लापता कर देना चाहते हैं क्योंकि वे उस गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से बच सकें जिससे वे घिरे हुए हैं। ‘सचमुच मुझे दण्ड दो कि हो जाऊँ, पाताली अँधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएँ के बादलों में, बिलकुल मैं लापता!!’ लेकिन कवि के लिए यह पलायन भी संभव नहीं है क्योंकि जहाँ भी वे जाएँगे, वहाँ भी उनका अतीत, उनकी चेतना, उनकी विचारधारा उनका पीछा करती रहेगी। ‘लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है!!’ यहाँ “तुम” एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ‘तुम’ एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई विचारधारा भी हो सकती है और यहाँ तक कि समाज भी हो सकता है। मुक्तिबोध इस विचार से बचना चाहते हैं लेकिन यह इतना सर्वव्यापी और गहरा है कि वे इससे कभी मुक्त नहीं हो सकते।
आत्मीयता की असहनीयता:
कवि के हृदय पर संवेदनशीलता का इतना प्रभाव है कि अब आत्मीयता, ममता और अपनापन भी उनके लिए पीड़ादायक हो गया है। ‘ममता के बादल की मँडराती कोमलता, भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है’ यहाँ कवि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनकी संवेदनशीलता और आत्मीयता उनके लिए कमजोरी बन सकती है। यह समाज में व्याप्त क्रूरता और कठोरता को भी दर्शाता है, जहाँ बहुत अधिक संवेदनशील होना व्यक्ति के लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर सकता है।
सामाजिक चेतना और विचारधारा की अनिवार्यता:
कविता के अंत में मुक्तिबोध इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका अस्तित्व केवल उनके अपने कारण नहीं बल्कि किसी बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक परिवेश के कारण है। ‘सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है।’ यहाँ वे स्वीकारते हैं कि उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनकी संवेदना सब कुछ किसी और की प्रेरणा से ही आकार लेती है। यह विचारधारा मार्क्सवादी चेतना से भी जुड़ती है। ‘अब तक तो ज़िन्दगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है।’ यहाँ अंतिम पंक्तियाँ पुनः इस विचार को पुष्ट करती हैं कि कवि का समर्पण केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस व्यापक शक्ति (संभावित रूप से समाज, विचारधारा या क्रांतिकारी चेतना) के लिए है।
कविता की काव्यगत विशेषताएँ:
- बिंबात्मकता: कविता में चंद्रमा, ध्रुवीय अंधकार, ममता के बादल, धुएँ के बादल जैसे बिंब मानसिक स्थितियों को स्पष्ट करते हैं।
- प्रतीकात्मकता: ‘तुम’, ‘अंधकार’, ‘सहर्ष स्वीकारा’ आदि गहरे प्रतीक हैं जो आत्मसंघर्ष, सामाजिक चेतना और विचारधारा को दर्शाते हैं।
- भावनात्मक तीव्रता: कविता में आत्मीयता, संघर्ष और बेचैनी के भाव अत्यंत तीव्रता से व्यक्त हुए हैं।
- मार्क्सवादी चेतना: व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को उजागर करना मुक्तिबोध की विचारधारा का एक प्रमुख तत्व है।
निष्कर्ष:
प्रस्तुत कविता ‘सहर्ष स्वीकारा है’ केवल एक आत्मस्वीकृति की ही कविता नहीं बल्कि यह एक बौद्धिक, दार्शनिक और सामाजिक आत्मनिरीक्षण की कविता भी है। मुक्तिबोध इस कविता में अपनी संवेदनशीलता, अपने संघर्ष, अपने विचारों की तीव्रता और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं।वे यह मानते हैं कि उनका जीवन संघर्षों और द्वंद्वों से भरा हुआ है लेकिन वे इसे नकारते नहीं बल्कि इसे ‘सहर्ष स्वीकारते हैं’ क्योंकि यही उनकी पहचान है। कविता में व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना का द्वंद्व, आत्मीयता की असहनीयता और विचारधारा से जुड़े रहने की अनिवार्यता को गहरी संवेदनशीलता और मार्मिकता से चित्रण किया गया है।